सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005: पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना।
महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, औरंगाबाद में तीसरे वर्ष की छात्रा दिव्यांजली मिश्रा और गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, मुंबई में दूसरे वर्ष के छात्र हर्ष जादौन|
12/16/20241 min read
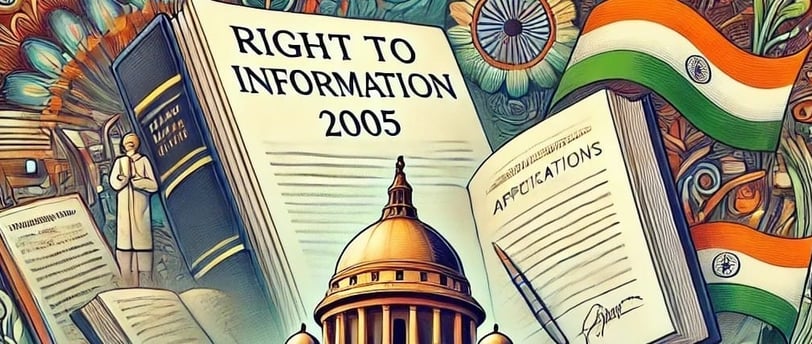
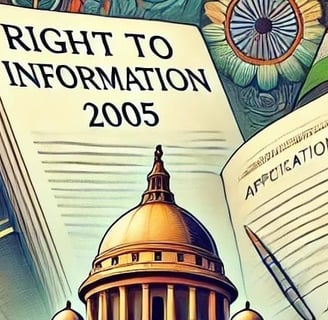
उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज नारायण (1975) के प्रमुख मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत गारंटीकृत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में मान्यता दी। अदालत ने कहा कि एक कार्यशील लोकतंत्र में, सरकार की गतिविधियों के बारे में जानना नागरिकों का अधिकार है। इस लेख में, हम सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के महत्व, इसमें शामिल अधिकारियों, शुल्क, प्रारूप, अपील और आर. टी. आई. दाखिल करने के लिए छूट पर प्रकाश डालेंगे।
सूचना अधिनियम, 2005 का अधिकार क्या है?
सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 बनाया जिसके माध्यम से नागरिक सार्वजनिक प्राधिकरण से ऐसी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो सार्वजनिक प्राधिकरण के पास है या जो उसके नियंत्रण में है। "लोक प्राधिकारी" से संविधान के तहत स्थापित कोई भी संस्था अभिप्रेत है; संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई कोई अन्य विधि या उपयुक्त सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश।
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उद्देश्य
सूचना का अधिकार अधिनियम नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी लेने का अधिकार देता है।
यह अधिनियम सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
यह अधिनियम सार्वजनिक प्राधिकरणों के संचालन में भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने में भी मदद करता है।
जानकारी जिसकी आवश्यकता हो सकती है
सूचना का अधिकार (आर. टी. आई.) अधिनियम 2005 के प्रावधान भारतीय नागरिकों को अधिकारियों द्वारा रखे गए डेटा तक पहुंच का अनुरोध करने की अनुमति देते हैं।
जानकारी की एक श्रृंखला प्राप्त की जा सकती है जिसमें शामिल हैंः सरकारी नीतियों और जनता को प्रभावित करने वाले निर्णयों की जानकारी।
सरकारी विभागों और एजेंसियों का बजट और व्यय।
आधिकारिक रिकॉर्ड, रिपोर्ट, दस्तावेज, ईमेल, ज्ञापन और सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा रखी गई कोई भी अन्य प्रासंगिक जानकारी।
प्रभावित व्यक्तियों को सरकार के प्रशासनिक या अर्ध-न्यायिक निर्णयों के कारणों की जानकारी।
आर. टी. आई. की विशेषताएं
यह सार्वजनिक प्राधिकरणों को अधिनियम की धारा 4 में प्रदान किए गए अपने संगठन, कार्यों, कर्तव्यों आदि के विवरणों के संबंध में स्वतः (अपनी मर्जी से) प्रकटीकरण करने के लिए बाध्य करता है।
भारतीय नागरिक आर. टी. आई. अनुरोध या तो लिखित आवेदन पत्र में या सरकारी एजेंसी से मांगी गई जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से निर्दिष्ट कर सकते हैं। अनुरोध आवेदन के साथ, एक छोटा शुल्क भी देना पड़ता है।
यह अधिनियम सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, सरकारी विभागों, मंत्रालयों, गैर सरकारी संगठनों पर लागू होता है जिन्हें सरकार और संविधान द्वारा या कानून के माध्यम से स्थापित अन्य संस्थानों से पर्याप्त धन प्राप्त हुआ है।
नोटः व्यक्ति को जानकारी मांगने के लिए कारण देने की आवश्यकता नहीं है और न ही व्यक्ति को संपर्क करने के लिए आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी के अलावा अन्य जानकारी साझा करने की आवश्यकता है| यदि कोई आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (बी. पी. एल.) श्रेणी का है तो उसे कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है।
समयबद्ध जवाब और आवेदन
सरकारी एजेंसियों को आर. टी. आई. अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर उनका जवाब देना चाहिए। यदि अनुरोध की गई जानकारी किसी के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है, तो प्रतिक्रिया समय को घटाकर 48 घंटे कर दिया जाता है|
यदि कोई नागरिक जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो उसके पास प्रथम अपील प्राधिकरण (एफ. ए. ए.) में अपील दायर करने का विकल्प है।
पहली अपील उस तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर दायर की जानी चाहिए जिस दिन सूचना की आपूर्ति की 30 दिनों की सीमा समाप्त हो जाती है या उस तारीख से जिस दिन लोक सूचना अधिकारी की जानकारी या निर्णय प्राप्त होता है। अपीलीय प्राधिकारी अपील की प्राप्ति के 30 दिनों की अवधि के भीतर या 45 दिनों के भीतर असाधारण मामलों में अपील का निपटारा करेगा। (आर. टी. आई. अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1))|
केंद्रीय सूचना आयोग के साथ दूसरी अपील उस तारीख से 90 दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए जिस दिन निर्णय पहले अपीलीय प्राधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए था या वास्तव में अपीलार्थी द्वारा प्राप्त किया गया था। आर. टी. आई. अधिनियम, 2005 की धारा 19 (3) (धारा 7 (5))|
आर. टी. आई. दाखिल करने के लिए अपवाद
आवेदकों को भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों से संबंधित जानकारी को छोड़कर धारा 8 और 9 के तहत छूट प्राप्त जानकारी और दूसरी अनुसूची में शामिल संस्थानों से भी बचना चाहिए। (आर. टी. आई. अधिनियम, 2005 की धारा 8,9)|
महत्वपूर्ण वेबसाइट
भारत सरकार (http://indiaimage.nic.in)
सूचना का अधिकार पोर्टल (www.rti.gov.in)
केंद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट (http://cic.gov.in)
आर. टी. आई. कौन दायर करेगा?
जानकारी चाहने वाले नागरिकों को संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सी. पी. आई. ओ.) को आवेदन करना होता है। आवेदन लिखित में होना चाहिए और भाषा हिंदी, अंग्रेजी या उस क्षेत्र की आधिकारिक भाषा में हो सकती है जिसमें आवेदन किया गया है। आवेदन में आवश्यक जानकारी निर्दिष्ट की जानी चाहिए। और फिर आवश्यक न्यूनतम शुल्क का भुगतान करना पड़ा जैसा कि ऊपर चर्चा की गई थी|
कैसे पता चले कि सी. पी. आई. ओ. कौन है? सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों ने अपने सी. पी. आई. ओ. को नामित किया है और सी. पी. आई. ओ. के बारे में आवश्यक जानकारी अपनी वेबसाइटों पर पोस्ट की है। इसे 'आर. टी. आई. पोर्टल' (www.rti.gov.in) पर देखा जा सकता है। इसके अलावा, यदि सी. पी. आई. ओ. का नाम संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण की वेबसाइट पर नहीं मिलता है, तो सार्वजनिक प्राधिकरण के पते पर नाम निर्दिष्ट किए बिना सी. पी. आई. ओ. को आवेदन भेजा जा सकता है|
नोटः यदि कोई व्यक्ति लिखित में अनुरोध करने में असमर्थ है, तो वह अपना आवेदन लिखने के लिए सी. पी. आई. ओ. की मदद ले सकता है।
निष्कर्ष
2005 का आर. टी. आई. अधिनियम एक महत्वपूर्ण कानून है जो शासन में जवाबदेही, पारदर्शिता और नागरिक सशक्तिकरण जैसे मूल्यों को बरकरार रखता है। यह शासन में प्रतिक्रियाशीलता और विश्वास को बढ़ावा देता है। हालांकि, आर. टी. आई. अनुरोधों को संबोधित करने में देरी से निपटने, अधिनियम के बारे में नागरिकों के बीच जागरूकता बढ़ाने और कानून के किसी भी दुरुपयोग या शोषण को रोकने के लिए इसके कार्यान्वयन के लिए तंत्र को बढ़ाने जैसी समस्याएं हैं। अधिनियम के सिद्धांतों को शामिल करके और इसके निष्पादन की दिशा में काम करके हम एक सुशिक्षित लोकतांत्रिक समाज के पोषण में इसके लाभों को उजागर कर सकते हैं|
Rights
Empowering individuals with legal updates.
Duties
Law
+917078214478
© 2024. All rights reserved.
lawblogs@kanoonkehaath.in
